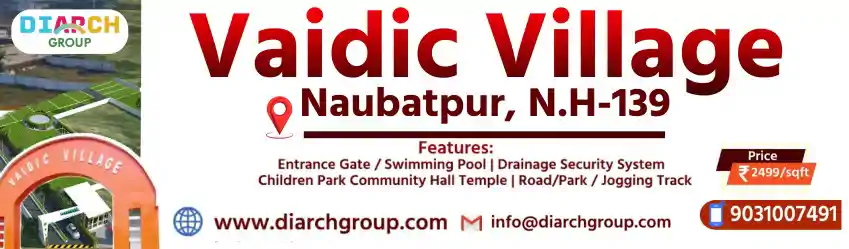Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र, राष्ट्रपति-राज्यपाल की शक्तियों पर टकराव, केंद्र ने कहा- न्यायपालिका हर संवैधानिक पेचीदगी का समाधान नहीं दे सकती
Supreme Court: राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी अथवा रोक लगाने की समयसीमा तय करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने तीखी आपत्ति जताई है।

Supreme Court:भारत के संवैधानिक ढांचे में एक नई बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर मंजूरी अथवा रोक लगाने की समयसीमा तय करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने तीखी आपत्ति जताई है। केंद्र का कहना है कि न्यायपालिका ने अपनी सीमा से बाहर जाकर ऐसा कदम उठाया है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को अस्थिर कर सकता है।
दरअसल, 8 अप्रैल को जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल विधेयकों पर अनिश्चित काल तक चुप्पी साधे नहीं रह सकते। अदालत ने निर्णय की समयसीमा तय की और तमिलनाडु के 10 विधेयकों को “डिम्ड असेंट” (स्वीकृत माने जाना) घोषित कर दिया।
केंद्र ने अपनी लिखित दलीलों में कहा कि न्यायपालिका हर संवैधानिक पेचीदगी का समाधान नहीं दे सकती। यदि ऐसा हुआ तो तीनों अंगों के बीच संस्थागत पदानुक्रम स्थापित हो जाएगा। अनुच्छेद 142 अदालत को ऐसी शक्तियां नहीं देता कि वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णयों पर सीमा तय करे। यह तो संवैधानिक प्रक्रिया को उलटने जैसा है।
तीनों अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—एक ही संवैधानिक स्रोत से शक्ति प्राप्त करते हैं। इनमें से किसी को भी दूसरों पर सर्वोच्च नहीं माना जा सकता।
केंद्र का मानना है कि विधेयकों पर सहमति या आपत्ति की प्रक्रिया राजनीतिक और लोकतांत्रिक उपायों से हल होनी चाहिए, न कि न्यायिक आदेशों से। उसने जोर देकर कहा कि जहां संविधान ने आवश्यक समझा है, वहां समयसीमा का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद 200 और 201 में ऐसी कोई समयसीमा नहीं दी गई। ऐसे में अदालत द्वारा समयसीमा तय करना असंवैधानिक है।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस रुख पर भी नाराज़गी जताई, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई थीं। केंद्र ने कहा कि राज्यपाल न तो राज्यों में बाहरी व्यक्ति हैं और न ही केवल केंद्र के दूत। वे राष्ट्रीय हित और लोकतांत्रिक भावना के प्रतिनिधि हैं।
यह विवाद भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा को झकझोरता है। जहां न्यायपालिका पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर समयसीमा लागू करना चाहती है, वहीं केंद्र इसे संविधान के ‘संतुलन सिद्धांत’ पर आघात मानता है। सवाल यही है कि क्या न्यायपालिका लोकतंत्र की संरचना में “सर्वोच्च निर्णायक” बन सकती है, या फिर यह जिम्मेदारी राजनीतिक विमर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की होनी चाहिए?